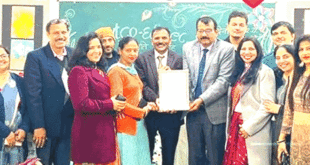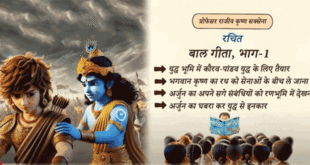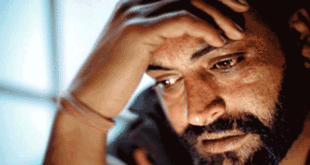Innocence and humanity of village societies is distinct from the clever selfishness of cities. Here is a nice poem by Kunwar Bechain depicting this fact. Rajiv Krishna Saxena
अंतर
मीठापन जो लाया था मैं गाँव से
कुछ दिन शहर रहा अब कड़वी ककड़ी है।
तब तो नंगे पाँव धूप में ठंडे थे
अब जूतों में रह कर भी जल जाते हैं
तब आया करती थी महक पसीने से
आज इत्र भी कपड़ों को छल जाते हैं
मुक्त हँसी जो लाया था मैं गाँव से
अब अनाम जंजीरों ने आ जकड़ी है।
तालाबों में झाँक सँवर जाते थे हम
अब दर्पण भी हमको सजा नहीं पाते
हाथों में लेकर जो फूल चले थे हम
शहरों में आते ही बने बहीखाते
नन्हा तिल जो लाया था मैं गाँव से
चेहरे पर अब जाल पूरती मकड़ी है।
तब गाली भी लोकगीत सी लगती थी
अब यक़ीन भी धोकेबाज़ नज़र आता
तब तो घूँघट तक का मौन समझते थे
अब न शोर भी अपना अर्थ बता पाता
सिंह गर्जना लाया था मैं गाँव से
अब वह केवल पात चबाती बकरी है।
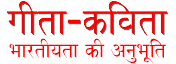 Geeta-Kavita Collection of Hindi poems & articles
Geeta-Kavita Collection of Hindi poems & articles